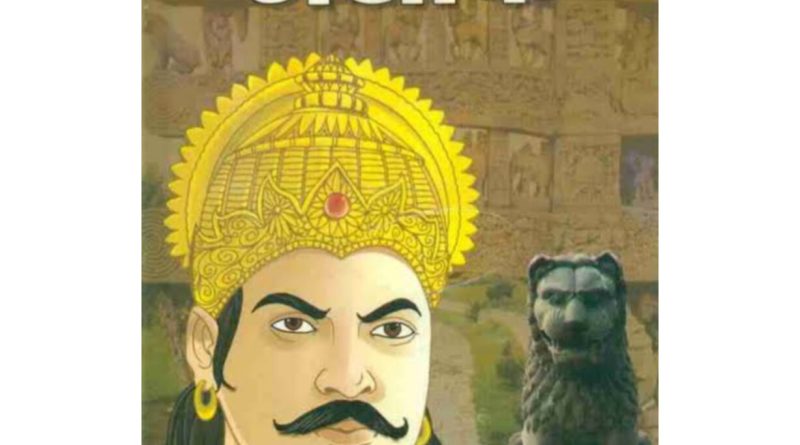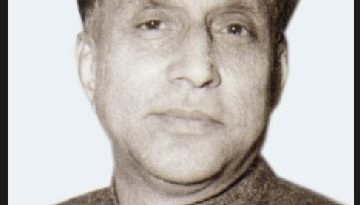शोध पत्र: “सम्राट अशोक राज्य कालखंड में मानवाधिकार के उजले पृष्ठ” – एक सिंहावलोकन
● डॉ उषा अग्रवाल, मंदसौर
देश राज्य और विश्व मे मानव अधिकारों पर वर्तमान और प्राचीन काल मे महत्व रहा है । इस संदर्भ में सम्राट अशोक के राज्य में तत्कालीन कालखंड में भी मानव अधिकारों का विस्तृत उल्लेख सामने आया है ।
प्रस्तुत शोध पत्र में मानव अधिकारों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तीसरी शताब्दी ई.पू. के भारत की पृष्ठभूमि में देखने की कोशिश की गई। भारतीय इतिहास में जिन प्रमुख व्यक्तियों ने देश की गतिविधि और परिवर्तन की विविध धाराओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, उनमें अशोक का एक विशिष्ट स्थान है। विभिन्न लोग उसे विभिन्न रूपों में देखते है। किसी को वह विजेता दिखाई देता है जिसने विजय के दुष्परिणामों से द्रवित होकर उसे सदा के लिए त्याग दिया। किसी को वह संत दिखाई देता है तो किसी को सन्यासी व सम्राट का मिश्रण नजर आता है। कोई उसे महान राजनीतिज्ञ मानता है। हमारे सामने उसकी जो तस्वीर उभरती है वह है मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में। यद्यपि मानव अधिकार की अवधारणा 1215 के इंग्लैण्ड के मैग्नाकार्टा से मानी जाती है, किन्तु इसमें समाहित मूल भाव के अनुसार कार्य तो ई.पू. तीसरी शताब्दी में ही अशोक ने कर दिखाया था। इस प्रकार मानव अधिकारों के प्रथम संरक्षण के रूप में हम भारतीय इतिहास में अशोक को पाते हैं।
व्यक्ति को मानव अधिकार प्रदान करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इनमें मानव की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा का अधिकार एवं न्याय का अधिकार प्रमुख है। ये अधिकार जाति, धर्म, राष्ट्र के भेदभाव से हट हर व्यक्ति को अपने स्वयं के अस्तित्व को जीने का अधिकार है। प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि अशोक के विचारों और कार्यों में ये अधिकार कितना महत्व रखते थे और इन अधिकारों को वह अपनी प्रजा को प्रदान करने में कहां तक सफल हुआ।
इस अध्ययन में अशोक के शिलालेखों को आधार बनाया गया है, जो उसने अपने 36 वर्ष के सुदीर्घ शासन काल में समय-समय पर फरमान व प्रजा के नाम सम्राट की घोषणा के रूप में खुदवाये थे। इनमें 14 बडे शिलालेख है जो कालसी, मानसेहरा, शहबाजगढी, गिरनार, सोपारा, येर्रगुडी, धौली और जौगढ में पाये गये है। कतिपय छोटे शिलालेख वैराठ, रूपनाथ, सहसराम, ब्रहमगिरी, गोविमठ, जटिंगरामेश्वर, मास्की, पालकीगुण्ड, राजुल, मण्डगिरी, सिद्धपुर, गुर्जरा और बुधनी, पानगोरिया की पहाड़ी गुफाओं में पाये गये। इसी प्रकार सात स्तूप लेख इलाहाबाद, दिल्ली-तोपरा, दिल्ली-मेरठ, लौरिया-अरराज, लौरिया, नन्दनगढ और रामपुरवा में भी पाये गये। अन्य अभिलेख सांची, सारनाथ तथा वैराठ में पाये गये है। इन सभी शिलालेखों में राज्यादेश प्रियदस्सी की आज्ञा से लिखे गये थे जो अशोक की उपाधि थी। इन अभिलेखों को महत्वपूर्ण स्थानों, नगरों के निकट प्रसिद्ध व्यापारिक और यात्रा मार्गों पर या धार्मिक स्थानों पर उत्कीर्ण करवाया गया था।
अशोक की सबसे बडी उपलब्धि उसकी धम्म नीति की अवधारणा थी। यह नीति किसी धर्म को अपनाने की मांग करने के बजाय सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति थी। उसकी कोशिश ऐसा दृष्टिकोण पैदा करने की थी जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाये।
इस धम्म नीति में मनुष्य की गरिमा पहचानने पर और समाज की गतिविधियों में मानवतावादी भावना पर बल दिया गया, जो आज के मानव अधिकार की अवधारणा की मूल भावना है। अशोक ने अपने दूसरे तथा सातवें स्तम्भ लेख में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है – धम्म है, साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। आगे कहा गया है प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता-पिता तथ बडों की आज्ञा मानना। गुरूजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार। अशोक ने अपने अंतिम सार्वजनिक घोषणा सातवें स्तम्भ लेख (देहली टोपरा) में कहा है: ’’जो कुछ मैने किये हैं, लोगों ने उसे स्वीकार किया है और उनका अनुसरण किया है। इसलिये माता-पिता की आज्ञा का पालन, गुरूजनों की आज्ञापालन, वृद्धजनों का सत्कार, ब्राह्मणों और श्रमणों, गरीबों और दुखियों दास और नौकरों के साथ उचित व्यवहार बढा है और बढेगा।’’
इस प्रकार मानव अधिकार चार्टर की प्रस्तावना में जो मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व की बात कही गई, वह अशोक धम्म नीति से उसके कार्यकाल में क्रियान्वित भी हुई है।
अशोक न केवल सभी इंसानों की समानता में विश्वास रखता था वरन उसने न्याय प्रणाली व दंड विधान में भी समानता पर जोर दिया। अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद चौथा स्तम्भ लेख उत्कीर्ण करवाया था। इसमें वह कहता है कि मैने ग्रामवासियों के लिए और सुख के लिए राजूकों को नियुक्त किया है और मैने न्याय और दंड में उन्हें पुरी स्वतंत्रता दी है। लेकिन यह वांछनीय है कि न्याय, विधि और दंड में एकरूपता हो।
यह एक अभूतपूर्व कदम था और यह बताता है कि अशोक सामाजिक न्याय को कितना महत्वपूर्ण मानता था।
इसी स्तम्भ लेख में वह कहता है कि ’’जो लोग कैद है या जिन्हें मौत की सजा दी गई है, उन्हें तीन दिन की मोहलत दी जाये। इस तरह उनके संबंधी उनके जीवनदान के लिए प्रार्थना कर सकते है या अगर उनके लिए निवेदन करने वाला कोई नहीं है तो वे दान दे सकते है या उपवास रख सकते हैं।’’
अशोक के पांचवे स्तम्भ लेख से पता चलता है कि उसके राज्याभिषेक के समय से 26 वर्षों तक (उसकी वर्षगाँठ) पर पच्चीस बार कैदियों को रिहा किया गया।
इतना ही नहीं उसने अपने पांचवे शिलालेख (कालसी) में कहा है कि मेरे महामात्र उन कैदियों को जिन्हें अन्यायपूर्वक बंदी बनाया गया है, वे उनके कल्याण की अभिवृद्धि में रत हैं या जिनकी संतान है, जो पीडित हैं और जो वृद्ध हैं, उन्हें रिहा करवाने में व्यस्त हैं।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बंदीगृह न तो घोर यातना का स्थान था न सर्वनाश का घर, बल्कि बंदीगृह कुछ-कुछ सुधारगृह के अनुरूप थें। पांचवे शिलालेख में वह बंदी के परिवार की रक्षा के लिए महामात्रों को कहता है।
अशोक के पांचवे शिलालेख से उसकी लोक कल्याणकारी नीति एवं समानता के अधिकार की पुष्टि होती है। वह यहां दासों और स्वामियों के बीच संबंध और बंदियों के प्रति व्यवहार के संबंध में चिंतित दिखाई देता है।
अशोक यद्यपि बौद्ध धर्म का अनुयायी था किन्तु वह मानव के धर्म के अधिकार का पूरा आदर करता था। उसने किसी को बौद्ध धर्म अपनाने या उसके स्वयं के धम्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया। वह अपने अभिलेखों में श्रमणों और ब्राह्मणों को साथ-साथ ही समान आदर से उल्लेख करता है। बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सबसे ज्यादा बल सहिष्णुता पर दिया जो कि उसके अनुसार दो प्रकार की थी: स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता और साथ ही उनके विचारों तथा विश्वासों की सहिष्णुता।
अपने 12 वें शिलालेख (गिरनार) में उसने सभी धर्मों की पारस्परिक सहिष्णुता तथा श्रद्धा पर जोर दिया है। वह कहता है – ’’जो अपने धर्म का सम्मान करता है और दूसरे धर्मों का निरादर करता है और इस प्रकार अपने धर्म को यह बढाना चाहता है वह वास्तव में अपने धर्म को भी हानि पहुंचाता है। ऐसे मनुष्य में धर्म की वास्तविकता की कमी है, सभी धर्मों का सार है कि दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए।’’
अशोक की धार्मिक नीति के विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर भी मानती हैं कि – ’’अपने धर्म प्रचार के द्वारा अशोक ने धार्मिक आदेशों में निहित संकीर्ण मनोवृत्ति का सुधार करने, सबलों से दुर्बलों की रक्षा करने तथा सम्पूर्ण साम्राज्य में ऐसी व्यापक चेतना जागृत करने का प्रयत्न किया, जिसके संबंध में किसी भी सांस्कृतिक समूह को कोई आपत्ति न हों।’’
इतना ही नहीं उसने राज्य में मानव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व, विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किये गये। पांचवे दीर्घ शिलालेख से पता चलाता है कि उसकी नीति एवं कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उसने नम्र स्वभाव वाले दयालू सरकारी कर्मचारियों को हर पांचवे वर्ष राज्य के विभिन्न प्रांतों का दौरा करने भेजा। उनका काम सरकारी कर्मचारियों के कामों की जांच करना था, जिससे किसी प्रजाजन के साथ अन्याय न हो सके। उज्जैन व तक्षशिला के राजकुमारों को आज्ञा दी गई कि वे कम कम से कम हर तीसरे वर्ष इस प्रकार के कर्मचारियों को दौरे पर भेजें। कुछ समय पश्चात इन नियमों को स्थायी रूप देने के लिए ’’धर्म महामात्र’’ नामक अधिकारियों ने नया विभाग खोला। अशोक के पांचवे दीर्घ शिलालेख में जो उसने अपने शासन के 13 वें में वर्ष में खुदवाया था से पता चलता है कि इन धर्म महामात्रों का काम जनता के नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन का उत्थान करना था।
ये धर्म महामात्र समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक की पूरी श्रृंखला के रूप में व्याप्त थे जैसा कि अशोक स्वयं कहता है – ये गृहस्थ से सन्यासी तक व्याप्त है।
इससे स्पष्ट होता है कि उसके कार्य किसी समुदाय विशेष तक सीमित न होकर सम्पूर्ण समाज के लिए थे। वह समाज के विस्तार की माप सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं वरन सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर करता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपनी सारी प्रजा के बौद्ध धर्मान्तरण का प्रयास नहीं किया बल्कि सामाजिक आचरण में मानवतावाद के सचेत प्रयोग पर जोर दिया। अशोक का धम्म निश्चय ही एक ऐसा मार्ग था जो सांस्कृतिक स्तर के किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता था और इसका अंगीकरण देश भर में एकता ला सकता था।
स्त्रियों की भलाई के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्र नियुक्त किया।
अशोक ने राज्य कार्य में राज्य पद के पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने घोषित किया कि प्रजा उसकी संतान के समान है और जिस तरह वह अपनी संतान के इहलोक और परलोक के सुख की कामना करता है उसी तरह वह अपनी समस्त प्रजा के लिए कल्याण की कामना करता है। वह प्रजा के कार्य करने के लिए सदैव उद्यत रहता था। अपने छठे शिलालेख में उसने यह घोषणा की कि हर क्षण और हर स्थान पर चाहे वह रसोई घर में हो, अंतः पुर में हो अथवा उद्यान में मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करे, मैं जनता का कार्य करने से कभी भी नहीं अद्याता, मुझे प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए।
उसके दूसरे दीर्घ शिलालेख (गिरनार) से पता चलता है कि राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया था इसमें मनुष्यों के लिए चिकित्सा परिचर्या और पशुओं के लिए चिकित्सा परिचर्या सम्मिलित है। इतना ही नहीं औषधियों की जडी बूटियां जहाँ-जहाँ नहीं थीं, वहाँ-वहाँ लाई गई और रोपी गई, मार्गों में कुएं खुदवाए गए और वृक्ष लगवाए गए।
इस प्रकार आज जो हम स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी अधिकारों की अपेक्षा राज्य से रखते हैं वे स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण स्थापित करने का प्रयास उस युग में अशोक ने क्रियान्वित किया था।
कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध की नीति त्यागकर अशोक ने न केवल अपनी जनता को तीस वर्षों तक युद्ध मुक्त शांति का वातावरण प्रदान किया वरन पड़ोसी राज्यों को उससे आश्वस्त किया कि उससे उन्हें डरना नहीं चाहिए वह तो शांति पूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण करेगा।
अशोक ने पाश्चात्य देशों को भी अपने मानवीय कार्यों की परिधि में सम्मिलित किया और तेरहवें आदेश लेख में वर्णित अंतियोक (झिरिया), 2. तुरमय (मिश्र), 3. अंतिकिनी (मकदुनिया) 4. यक (सीरीज), 5. आठिकसुन्दरों नामक पांच पाश्चात्य राजाओं के राज्यों में दुख निवारण के निमित्त चिकित्सकों को मिशन भेजे। इन मिशनों की तुलना आधुनिक सदभावना मिशनों से की जा सकती है। पश्चिमी राज्यों के साथ-साथ, दक्षिणी राज्यों में भी धम्म विजय के प्रमाण मिलते है।
इन दक्षिणी राज्यों में चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र और श्रीलंका प्रमुख है। अशोक के तेरहवें शिलालेख के अनुसार इन सभी देशों में लोग धम्मानुशासन (धर्म की शिक्षा) सुनते हैं और धम्मानुकूल आचरण करते हैं।
धर्म महामात्र – दान धर्म संबंधी कार्यों का उच्चायुक्त
धर्म महामात्र – समदृष्टि का उच्चायुक्त
*राजस्व का अदभुत आदर्श -* ’’मैं जो कुछ पराक्रम करता हूँ वह इसलिये कि प्राणियों के प्रति मेरा जो ऋण है उससे उऋण हो जाऊँ।
● डॉ. उषा अग्रवाल
प्राध्यापक
इतिहास एवं पर्यटन विभाग
प्रधानमंत्री एक्सिलेंस कॉलेज मंदसौर